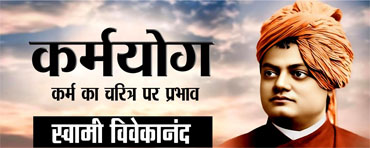
कर्म शब्द 'कृ' धातु से निकला है; 'कृ' धातु का अर्थ है करना । जो कुछ किया जाता है, वही कर्म है । इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ 'कर्मफल' भी होता है । दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाय, तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं, जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं । परन्तु कर्मयोग में 'कर्म' शब्द से हमारा मतलब केवल 'कार्य' ही है । मानवजाति का चरम लक्ष्य ज्ञानलाभ है । प्राच्य दर्शनशास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है । मनुष्य का अन्तिम ध्येय सुख नहीं वरन् ज्ञान है; क्योंकि सुख और आनन्द का तो एक न एक दिन अन्त हो ही जाता है । अत: यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, मनुष्य की भारी भूल है । संसार में सब दुःखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख हो उसका चरम लक्ष्य है । पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है, वह सुख नहीं वरन् ज्ञान है, तथा सुख और दुःख दोनों ही महान् शिक्षक हैं, और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है, उतनी ही दुःख से भी । मुख और दुःख ज्यों ज्यों आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं, त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते है । और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का 'चरित्र' कहते हैं । यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो, तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है । तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्रगठन में सुख और दुःख दोनों ही समान रूप से उपादान- स्वरूप हैं | चरित्र को एक विशिष्ट ढाँचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है । पुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें, तो मैं कह सकता हूँ कि अधि- कांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुःख ने तथा ने सम्पत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है एवं प्रशंसा की अपेक्षा निन्दारूपी आघात ने ही उसकी अन्तःस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है ।
अब, यह ज्ञान मनुष्य में अन्तर्निहित है । कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अन्दर ही है । हम जो कहते हैं कि मनुष्य 'जानता ' है उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमे कहना चाहिए कि वह 'आविष्कार करता' है । मनुष्य जो कुछ 'सीखता' है, वह वास्तव में 'आविष्कार करना' ही है । 'आविष्कार' का अर्थ है -- मनुष्य का अपनी अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना । हम कहते हैं कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया । तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था ? नहीं, वह उसके मन में ही था । जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला | संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है, वह मन से ही निकला है । विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है । बाह्य जगत् तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है; परन्तु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है । सेव का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारणस्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया । उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव - शृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उनमें एक नयी कड़ी का आविष्कार किया । उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं । यह न तो सेव में था और न पृथ्वी के केन्द्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही । अतएव समस् ज्ञान, चाहे वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है । बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है । और जब आवरण धीरे-धीरे हटता जाता है, तो हम कहते है कि 'हमें ज्ञान हो रहा है' । ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है । जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है, वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है, वह अज्ञानी है । जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिलकुल चला जाता है, वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है अतीत मे कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है। कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असख्य पुरुष जन्म लेगे । जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े मे अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है । उद्दीपक- कारण घर्षणस्वरूप ही उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है । ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यो के सम्बन्ध में भी है । यदि हम शान्त होकर स्वयं का अध्ययन करे, तो प्रतीत होगा कि हमारा हँसना - रोना, सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, हमारी शुभ कामनाएँ एवं शाप, स्तुति और निन्दा ये सब हमारेमन के ऊपर बहिर्जगत् के अनेक घात-प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है । ये सब घात-प्रतिघात मिलकर 'कर्म' कहलाते हैं । आत्मा की आभ्यन्तरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाये जाते हैं, वे ही कर्म हैं । यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है । इस प्रकार, हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे वातचीत कर रहा हूँ -- यह कर्म है, तुम सुन रहे हो --- यह भी कर्म है; हमारा साँस लेना, चलना आदि भी कर्म है; जो कुछ हम करते हैं, वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है; और हमारे ऊपर वह अपना चिह्न अंकित कर जाता है ।
कई कार्य ऐसे भी होते है, जो मानो अनेक छोटे-छोटे कर्मों की समष्टि हैं । उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुनें, तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है । परन्तु हम जानते है कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी-छोटी लहरो से बनी है । और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परन्तु फिर भी वह हमे सुन नहीं पड़ता । पर ज्योंही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते है, त्योंही हमे बड़ी आवाज सुनायी देती है । इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है । कई कार्य ऐसे होते है, जिनका हम अनुभव करते है; वे हमारे इन्द्रियग्राह्य हो जाते है, पर साथ ही वे अनेक छोटे-छोटे कार्यों की समष्टिस्वरूप हैं । यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जाँचना चाहते हो, तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जाँच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है | मनुष्य के अत्यन्त साधारण कार्यो की जाँच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं, जिनसे तुम्हें एक महान् पुरुष वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है । आकस्मिक अवसर तो छोटे-से-छोटे मनुष्य को भी किसी-न-किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं | परन्तु वास्तव में बड़ा तो वही है, जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान् रहता है ।
मनुष्य का जिन सब गक्तियों के साथ सम्बन्ध आता है, उनमें से कर्मों की वह शक्ति सब से प्रवल है, जो मनुष्य के चरित्रगठन पर प्रभाव डालती है । मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केन्द्र है, और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है, तथा इस केन्द्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में केन्द्र ही 'प्रकृत मानव' ( आत्मा ) है; बाहर भेज रहा है । यह यह सर्वशक्तिमान् तथासर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है । भला- बुरा, सुख-दुःख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं, और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं । और वह उन सब में से चरित्र - रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है । जिस प्रकार किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है ।
संसार में हम जो सब कार्य-कलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सारा-का-सारा केवल मन का ही खेल है -- मनुष्य की इच्छा- शक्ति का प्रकाश मात्र है । अनेक प्रकार के यन्त्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छाशक्ति के विकास मात्र हैं । मनुष्य की यह इच्छाशक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है । अतएव, कर्म जैसा होगा, इच्छाशक्ति का विकास भी वैसा ही होगा । संसार में प्रबल इच्छाशक्ति सम्पन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरन्धर कर्मी थे । उनकी इच्छाशक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट-पुलट कर सकते थे । और यह शक्ति उन्हें युग-युगान्तर तक निरन्तर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी । बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छाशक्ति थी, वह एक जन्म में प्राप्त नही की जा सकती। और उसे हम आनुवंशिक शक्तिसंचार भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमे ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे । हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुँह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो । जोसेफ ( ईसा मसीह के पिता) के समान तो असंख्य बढ़ई हो गये और आज भी हैं; बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे-छोटे राजा हो चुके है । अतः यदि वह बात केवल आनुवंशिक शक्तिसंचार के ही कारण हुई हो, तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे, ऐसा एक सुन्दर पुत्र रत्न लाभ हुआ, जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है ? इसी प्रकार, जोसेफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूज जानेवाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अन्तर है, उसका स्पष्टीकरण कहाँ ? आनुवंशिक शक्तिसंचार के सिद्धान्त द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नही हो सकता । बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गये, वह आयी कहाँ से ? उस महान् शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ ? अवश्य, युग-युगान्तरों


Comments
Hanson Deck
Norman Gordon
Jake Weary